तालिबान की कल्पना में एक नैतिक समाज का निर्माण करना था वैसे जैसे पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद ने अरब के भ्रष्ट शासकों के ख़िलाफ़ विद्रोह किया और असभ्य समाज को सभ्य बनाने का काम किया। इसलिए उसे किसी संगठन और संस्था से ज़्यादा एक करिश्माई नेतृत्व की ज़रूरत थी। वैसे जैसे पैग़म्बर का नेतृत्व था। वह उसे मुल्ला उमर में मिला। जो सादगी पसन्द था और लड़ना भी जानता था और जिसमें आध्यात्मिक शक्ति भी थी। तालिबान की सफलता के पीछे बड़ा कारण यही है कि उसने अफ़ग़ानिस्तान की विविधताओं से लड़ते हुए भी उसे सबसे ज़्यादा अपने भीतर समाहित किया। जबकि अहमद शाह मसूद की पार्टी ज़मायत-ए-इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित होने के बावजूद लोगों को एकजुट नहीं कर पायी। दरअसल वे अफ़ग़ानी समाज में एकता ऊपर से थोपना चाहते थे जबकि तालिबान ने नीचे से एकता क़ायम की।

इसका मतलब यह नहीं है कि तालिबान से पहले अफ़ग़ानिस्तान में इस्लाम को मानने वाली संस्कृति नहीं थी। वह थी, लेकिन इस्लामी उग्रवाद नहीं था। तालिबान ने उस रूप को बदल दिया। ‘इस्लाम अफ़ग़ानी लोगों के जीवन में लम्बे समय से रहा है। आम अफ़ग़ानी रोज़ा, नमाज़ और जकात करते रहे हैं। अफ़ग़ानी समाज विविधतापूर्ण समाज रहा है। वहाँ पश्तून, ताज़िक, उज़्बेक, हाज़रा, हेराती, हिन्दू, सिक्ख और यहूदी समाज के लोग मिल-जुलकर रहते रहे हैं, लेकिन इस्लाम इस समाज को जोड़ता था। गाँव के केन्द्र में मस्जिद होती थी और बहुत सारी गतिविधियाँ उससे बँधी होती थीं, लेकिन जिहाद ने अफ़ग़ानियों के जीवन में ख़ास तरह के जोश और जज़्बे का संचार किया और उसी से उन्होंने पहले अंग्रेज़ों को तीन बार हराया फिर सोवियत संघ की सेना को भगाया और बाद में अमेरिका समेत नाटो की सेना को भी वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया।’
अफ़ग़ानी समाज किस कद्र इस्लाम के नियमों का पाबन्द रहा है इसका नमूना पेश करते हुए अहमद राशिद बताते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान पर चालीस साल तक (1933-1973) शासन करने वाले आख़िरी बादशाह मुहम्मद ज़हीर शाह का इंटरव्यू लेने 1988 में रोम गया। वहाँ इंटरव्यू के दौरान जैसे ही नमाज़़ का वक़्त होता था तो वे उठ कर बगल वाले कमरे में चले जाते थे। ज़हीर शाह ही क्यों अफ़ग़ानिस्तान के कम्युनिस्ट शासक भी अपने दफ़्तर में नमाज़ का कक्ष बनाये हुए थे और जब भी वक़्त होता था तो वे सरकारी कामकाज को विराम देकर नमाज़ अदा करने लगते थे। इसी तरह मुज़ाहिदीन लड़ाई रोक कर नमाज़ अदा करते थे। ऐसा भारत के मुगल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में भी कहा जाता है। वह युद्ध के मैदान में ही अपनी चटाई बिछाकर नमाज़ अदा करने लगता था। इससे एक ओर ऐसा करने वालों की धार्मिक आस्था का पता चलता है तो दूसरी ओर अल्लाह में उनके भरोसे का भी।

मुल्ला उमर अपनी नमाज़ की चटाई पर घण्टों बिताता था। कहते हैं कि उस दौरान उसे तमाम फैसले लेने की सूझ आती थी। एक तरह से इलहाम होता था। यह सब होने के बावजूद अफ़ग़ानी समाज की खासियत यह थी कि कोई भी नमाज़ी बगल वाले से यह नहीं कहता था कि चलो तुम भी नमाज़़ पढ़ो। यानी नमाज़ पढ़ने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाता था। अफ़ग़ानिस्तान में इस्लाम रहा है और लम्बे समय से रहा है, लेकिन वह ऐसा कट्टर नहीं था जैसा आज है। वह सहनशील रहा है। वह दूसरे पन्थों और धर्मों के लिए आक्रामक नहीं रहा है। अफ़ग़ानी मुल्ला कभी किसी पर अपना मज़हब थोपते नहीं थे। यही वजह थी कि सन् 1992 तक हिन्दू, सिक्ख और यहूदी देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते थे। हिन्दू और सिक्ख वही थे जो अंग्रेज़ों के हमलों के दौरान 1839, 1879 और बाद में 1919 में उनके सैनिक और सहायक बनकर अफ़ग़ानिस्तान गये थे। उनमें से बहुतेरे तो मार दिये गये और जो बचे वे वहाँ बस गये थे। हिन्दू और सिक्ख मुगल बादशाहों और महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य के दौरान भी वहाँ गये थे जिसे कुछ समय के लिए अफ़ग़ानिस्तान तक विस्तार मिला था।
हिन्दू, सिक्ख और यहूदी अफ़ग़ानिस्तान के शहरों जैसे काबुल, कन्धार, हेरात और मज़ार के मुद्रा बाज़ारों को नियन्त्रित करते थे। वे लड़ाई के दौरान बादशाह को वित्तीय मदद देते थे जिसे बादशाह बाद में लौटाता था। यह एक ऐसी समझदारी थी जो किसी भी देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भाईचारे के लिए बुनियादी शर्त है, लेकिन 1992 के बाद वे वापस आ गये। वजह थी कि उसके बाद छिड़े गृहयुद्ध ने अफ़ग़ानी समाज की सहनशीलता को तोड़ दिया। ताज़िक नेता अहमद शाह मसूद ने 1995 में काबुल में हाजराओं यानी शियाओं को मारा। हाज़राओं ने 1997 में तालिबानियों यानी पश्तूनों को मज़ार-ए-शरीफ में मारा। तालिबानियों ने 1998 में हाजरा और उज़्बेकों को मारा। यह सारी मार-काट सामान्य नहीं थी। इसमें हज़ारों तालिबानियों, हाजराओं और उज़्बेकों का क़त्लेआम हुआ। यह लड़ाई से ज़्यादा नफरत की कहानी थी। उससे न सिर्फ़ जातीय विभाजन तेज हुआ बल्कि शिया सुन्नी विभाजन भी बढ़ गया।
इस्लाम में अल्लाह और पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद के मामले पर तो एकमत है, लेकिन उसके आगे ख़लीफ़ा और इमाम को लेकर बहुत विवाद है। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा विभाजन तो शिया और सुन्नी का है। हालाँकि सुन्नियों की आबादी 80-85 प्रतिशत है और शिया तक़रीबन 15-20 प्रतिशत। बाकी दूसरे सम्प्रदाय कम संख्या में हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी है और उनकी स्थिति बहुत ख़राब रहती है। इस्लाम के भीतर अहमदिया जैसे अल्पसंख्यक सम्प्रदाय की तो बड़ी बेकद्री है, लेकिन असली टकराव तो शिया और सुन्नी का होता है और सुन्नी लोग शिया को भी मुसलमान नहीं मानते। सुन्नियों का मानना है कि मुहम्मद साहेब के न रहने पर चार ख़लीफ़ा हुए जो उनके उत्तराधिकारी थे। उन्हें खुलफा-ए-राशिदीन यानी सही दिशा में चलने वाला बताया जाता है। इन ख़लीफ़ाओं के नाम हैं- अबू बकर (632-634), हज़रत उमर (634-644), हज़रत उस्मान (644-656) और हज़रत अली (656-661)। इनमें अबू बकर मुहम्मद साहेब के ससुर थे और हज़रत अली उनके दामाद। जबकि शियाओं का कहना है कि पैग़म्बर के बाद किसी को ख़लीफ़ा कहना उचित नहीं है। उसके बाद जो भी हुए उन्हें इमाम कहा जाना चाहिए। अबू बकर के बारे में शियाओं का कहना है कि मुहम्मद साहेब अपने दामाद हज़रत अली को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन अबू बकर ने धोखे से वह दर्जा हथिया लिया था। वे बाद में ख़लीफ़ा बने हज़रत अली को तो अपना नेता मानते है, लेकिन उससे पहले के तीन ख़लीफ़ाओं को नहीं मानते। इसलिए शिया और सुन्नी सम्प्रदाय में निरन्तर झगड़ा होता रहता है।
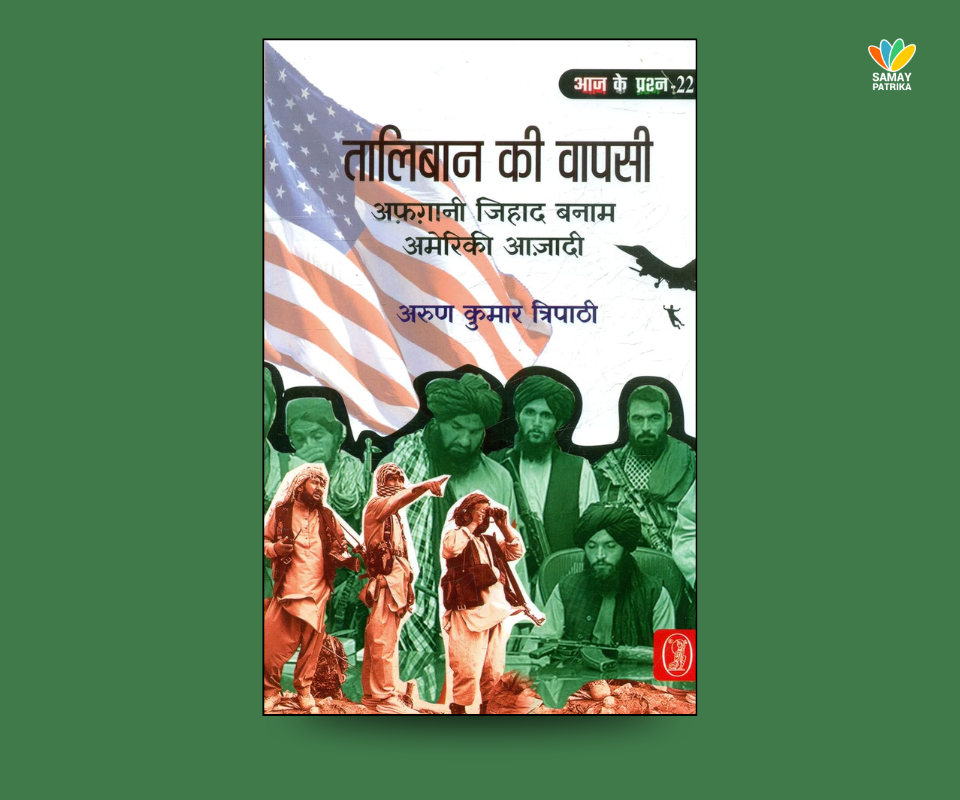
सुन्नियों के इसी पन्थ के भीतर चार मत यानी चार स्कूल हैं। वे चारों मत चार इमामों के आधार पर बने हैं। एक इमाम अबू हनीफा (699-767) हैं जिनके नाम पर हनफी मत बना। दूसरे हैं इमाम शाफई (767-820) जिनके नाम पर शाफई मत बना। तीसरे हैं इमाम हंबल (780-855)। उनके नाम पर हंबली मत बना। चौथे हैं इमाम मलिक (711-855)। उनके नाम पर मलिकी मत बना। इनमें से हंबली मत के लोग सऊदी अरब, कतर, कुवैत और मध्य पूर्व में पाये जाते हैं। वे इमाम का अनुसरण ज़रूरी मानते हैं। शाफई मत के लोग मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका में रहते हैं और अपने तौर तरीकों में हनफी मत के मानने वालों से अलग हैं। मालिकी मत के लोग इमाम मलिक की व्याख्या में विश्वास करते हैं और वे इमाम मोत्ता नामक किताब से अपनी व्याख्याएँ निकालते हैं। इस मत के लोग मध्यपूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका में रहते हैं। इन चारों मतों के अलावा सलफी, वहाबी और अहले हदीस मत के लोग भी होते हैं। इनमें सऊदी अरब के अल वहाब के नाम पर शुरू हुए वहाबी मत के लोग सबसे कट्टर माने जाते हैं। उनका कहना है कि किसी इमाम को मानना ज़रूरी नहीं है। विवाद होने की स्थिति में कुरान और हदीस के आधार पर फ़ैसला लिया जाना चाहिए।
इन चारों मतों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान में हनफी मत के लोग ज़्यादा पाये जाते हैं। वे तुलनात्मक रूप से उदार भी माने जाते थे। अफ़ग़ानिस्तान के सुन्नी भी ज़्यादातर हनफी ही रहे हैं।
भारत में हनफी मत के दो विभाजन हैं और इनका असर आसपास के देशों यानी पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान पर रहा है। हनफी मत के दो विभाजनों में एक है देवबन्दी और दूसरा है बरेलवी। यह दोनों मत उत्तर प्रदेश के दो शहरों के नाम पर हैं। बीसवीं सदी के आरम्भ में दो इमाम यानी इस्लामी विद्वान हुए जिनकी व्याख्याओं के आधार पर देवबन्दी और बरेलवी स्कूल की स्थापना हुई। उनमें से एक थे अशरफ अली थानवी (1863-1943)। दूसरे थे अहमद रजा बरेलवी (1856-1921)। इनमें से अशरफ अली थानवी की व्याख्या को मानने वालों ने देवबन्द की स्थापना की और अहमद रजा बरेलवी की बातों को मानने वालों ने बरेलवी स्कूल की स्थापना की। देवबन्दी लोग कुरान और हदीस को मानते हैं और बरेलवी भी उसे ही मानते हैं, लेकिन देवबन्दी किसी भी प्रकार की मज़ार और दरगाह में यक़ीन नहीं करते। वे शुद्ध मुहम्मद साहेब के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर चलने की बात करते हैं और उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं करते। एक तरह से उन पर वहाबी प्रभाव भी बताया जाता है। जबकि बरेलवी सूफ़ी मतों को भी मानते हैं और उनके परिसर में आला हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी की मज़ार भी है।

देवबन्द की स्थापना अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना कासिम ननौतवी ने 1866 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क़स्बे देवबन्द में की थी। गंगोही और ननौतवी दोनों शाह वली उल्लाह के शागिर्द थे और दिल्ली के मदरस-ए-रहीमिया के पढ़े थे। शाह वली उल्लाह इस्लाम के बड़े
विद्वान थे। 1987 के संग्राम में उनकी प्रेरणा भी मानी जाती है। गंगोही और ननौतवी दोनों ने 1857 की लड़ाई में योगदान दिया था। बाद में उन्होंने इस्लाम और उसकी संस्कृति के संवर्धन और पश्चिमी देशों के आक्रमण से बचाने के लिए देवबन्द में मदरसा कायम किया। यह मदरसा आज काहिरा के अल अजहर विश्वविद्यालय के बाद दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा इदारा है। आज दुनिया में तालिबान और अल-कायदा जैसे इस्लाम के उग्र और कट्टर रूप से मानने वालों को देवबन्द से ही प्रेरित बताया जाता है। पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में देवबन्दियों के मदरसों से निकले हुए छात्र ही मुज़ाहिदीन बने और बाद में तालिबान। हालाँकि देवबन्द इस नजरिये को हमेशा खारिज़ करता रहा है।
देवबन्द का एक दूसरा पहलू भारत के स्वाधीनता संग्राम में योगदान का भी रहा है। देवबन्द के मदरसे के तमाम उलेमा महात्मा गाँधी के सहयोगी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे। वे लगातार जेल भी गये और सजायें भी पायीं।
अफ़ग़ानिस्तान की 80 प्रतिशत आबादी सुन्नी मुसलमानों की है और वे हनफी मत के मानने वाले रहे हैं। इसे इस्लाम का उदार स्कूल माना जाता था। बाकी जो शिया आबादी है उसमें कुछ हाजरा, कुछ पश्तून, कुछ ताज़िक और कुछ हेराती लोग हैं। वहाँ इस्माइली समुदाय भी है जो आगा ख़ान के अनुयायी हैं। इस्माइली समुदाय भी तालिबान विरोधी हुआ करते थे, लेकिन तालिबान के विचारों को समझने के लिए तालिबान से पहले के समाज और बाद में बाहर से हुए हस्तक्षेप को समझना ज़रूरी है। सुन्नी हनफी पन्थ में ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं है। वह एक प्रकार से विकेन्द्रित है। वहाँ पर केन्द्रीकृत प्रणाली नहीं थी। या यूँ कहना चाहिए कि उसमें किसी एक धार्मिक नेता के पीछे चलने का रिवाज नहीं था। वहाँ नक्शबन्दी और कादिरिया नामक दो सूफ़ी तरीका (समुदाय) भी सक्रिय थे। सूफ़ीमत का जन्म इराक के बसरा शहर में 1000 साल पहले हुआ माना जाता है। सूफ का एक अर्थ होता है ऊन। जो लोग ऊनी कपड़े पहन कर इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे उन्हें सूफ़ी कहा गया। कुछ लोगों का कहना है कि सूफ़ी शब्द यूनान के सोफिस से बना है जिसका अर्थ होता है दर्शन यानी तसव्वुफ। इसलिए जो लोग रहस्य और दर्शन की बातें करते थे उन्हें सूफ़ी कहा गया। सूफियों को अहमियत अल-गजाली के समय में मिली। इनके प्रमुख सन्तों में राबिया, अल-अदहम, मन्सूर हल्लाज वगैरह थे। अत्तर, रूमी हाफिज़ जैसे मशहूर कवि भी सूफ़ी मत से ही थे।
मेरियन ब्रेमर कहती हैं कि अफ़ग़ानिस्तान के इतिहास में सूफ़ीवाद का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने समाज और राजनीति को गढ़ा है, लेकिन आज तालिबान के उभार के साथ बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी अहमियत क्या रही है। गाँव शहर दोनों जगहों की आबादी पर उनका असर रहा है। गजनी शहर में तो उनका केन्द्र रहा है। अफ़ग़ान बादशाह जब गद्दीनशीन होते थे तो सूफ़ी सन्त उस समय दुआ देने और मुबारकबाद देने के लिए मौज़्ाूद रहते थे, लेकिन सूफ़ी महज बादशाह बनाते नहीं थे, बल्कि वे अन्याय करने वाले बादशाहों के विरुद्ध विद्रोह भी करते थे। अमानुल्ला शाह के वक़्त में जब नये क़िस्म का क़ानून और संहिता का निर्माण होने लगा तो वे उनके ख़िलाफ़ हो गये। बाद में उनके तख़्तापलट में सूफियों का भी योगदान बताया जाता है।
इसे भी पढ़िए : भगवानदास मोरवाल का उपन्यास ‘दण्ड प्रहार’ संस्कृति, राष्ट्रवाद और संघर्ष का निर्मम आख्यान है
सोवियत कब्जे के विरुद्ध अफ़ग़ानी समाज को जगाने में सूफियों का बड़ा योगदान बताया जाता है। उन्होंने तमाम मुज़ाहिदीन गुटों को समर्थन दिया। एक सूफ़ी शेख और राजनेता सिगबतुल्लाह मुज़ाहिदी ने अफ़ग़ानिस्तान लिबरेशन फ्रंट का गठन किया और सोवियत सेनाओं से मोर्चा लिया। मुज़ाहिदी परिवार नक्शबन्दियों का नेता था और सदियों तक किंगमेकर की भूमिका में था। कम्युनिस्टों ने इस मुज़ाहिदी परिवार के 79 लोगों को काबुल में मार डाला। जनवरी 1979 में सिगबतुल्लाह मुजाहिदी ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफ़ग़ानिस्तान नाम से पार्टी बनायी। वह कट्टरपन्थियों का आलोचक था।
वे 1992 में दो महीने के लिए तब मुल्क़ के राष्ट्रपति बने जब नज़ीबुल्लाह का तख्तापलट हुआ। यानी वे देश के पहले मुजाद्दिदी राष्ट्रपति थे। उनके बाद बुरहानुद्दीन रब्बानी राष्ट्रपति बने, लेकिन जिन सूफियों ने सोवियत कब्जे से देश को आज़ाद कराने में मुज़ाहिदीन को खड़ा किया उन्हीं के गर्भ से निकले तालिबान ने उन्हें कुचल दिया। सन् 1996 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद सूफियों का दमन किया गया। सूफ़ियों की अच्छाई और बुराई यही है कि वे किसी से नफ़रत की बात नहीं करते। कम से कम सिद्धांत रूप में तो यही है। वे रूह और अल्लाह की बात करते हैं। इश्क हकीकी और इश्क मज़ाजी की बात करते हैं और इन्सान और अल्लाह के बीच एक मोहब्बत का रिश्ता कायम करते हैं। चिश्ती तरीका के सूफ़ी सन्त तो संगीत पर ज़ोर देते हैं।
यह बातें देवबन्दी ख़्याल को मानने वाले तालिबान को पसन्द नहीं थीं। इसलिए उन्होंने सूफ़ियों का दमन किया। 1996 से 2001 के बीच तो डर के मारे सूफ़ी भूमिगत हो गये। उसके बाद जब अमेरिका और यूरोप के समर्थन से हामिद करज़ई की सरकार बनी तो वे थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगे, लेकिन उन पर हमले जारी रहे और 15 मार्च 2012 को 11 सूफ़ी मारे गये। 2018 में भी 50 सूफ़ी विद्वान फिदायीन हमले में मारे गये।
~अरुण कुमार त्रिपाठी.
तालिबान की वापसी
अरुण कुमार त्रिपाठी
पृष्ठ : 312
वाणी प्रकाशन
किताब का लिंक : https://amzn.to/4826DKn
